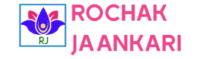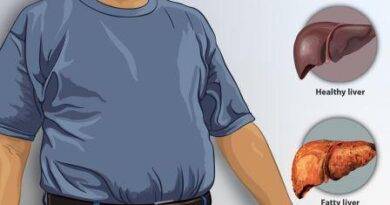Yoga -स्वरुप, प्रकार, प्रभाव तथा स्वस्थ व्यक्ति की दिनचर्या
 योग
योगऋषियों की मान्यताओं के अनुसार योग / Yoga का तात्पर्य स्वचेतना और चेतना के मुख्य केंद्र परमचैतन्य प्रभु के साथ संयुक्त हो जाना है।जैनाचार्यों के अनुसार जिन साधनों से आत्मा की सिद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है, वह योग है। अन्यत्र जैन दर्शन में मन वाणी एवं शरीर की वृतियों को ही कर्मयोग कहा गया है। इस लेख में हम Yoga के स्वरुप, प्रकार, प्रभाव तथा स्वस्थ व्यक्ति की दिनचर्या के बारे में चर्चा करेंगे।
Nature Of Yoga (योग का स्वरुप)
योग शब्द वेदों, उपनिषदों, गीता एवं पुराणों आदि में अति पुरातन काल से प्रयोग होता आया है। भारतीय दर्शन में योग एक अति महत्वपूर्ण शब्द है। आत्मदर्शन व समाधी से लेकर कर्मक्षेत्र तक योग का व्यापक व्यव्हार हमारे शास्त्रों में हुआ है। महर्षि व्यास योग का अर्थ समाधि बताते हैं। संयमपूर्वक साधना करते हुए आत्मा का परमात्मा के साथ योग करके (जोड़कर) समाधि का आनंद लेना योग है।
भारतीय ग्रंथों में गीता का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है। भारत के आधुनिक संतों ने गीता के योग का प्रचार विश्वभर में किया है। गीता में योगेश्वर श्री कृष्ण योग को विभिन्न अर्थों में प्रयोग करते हैं। अनुकूलता-प्रतिकूलता, सिद्धि-असिद्धि, सफलता-विफलता तथा जय-पराजय इन समस्त भावों में आत्मस्थ रहते हुए सम रहने को योग कहते है। निष्पक्ष भाव से द्रष्टा(आत्मा) बनकर अंतर की दिव्य प्रेरणा से प्रेरित होकर कुशलता पूर्वक कर्म करना गीता में योग ही माना है।
Types Of Yoga ( योग के प्रकार )
दत्तात्रेय योगशास्त्र तथा योगराज उपनिषद में मंत्रयोग, लययोग, हठयोग तथा राजयोग के रूप में योग के चार प्रकार माने गए हैं।
Mantr Yoga (मन्त्र योग)
मातृकारियुक्त मन्त्र को 12 वर्ष तक विधिपूर्वक जपने से अप्रिया आदि सिद्धियाँ साधक को प्राप्त हो जाती है।
Laya Yoga (लय योग)
दैनिक क्रियाओं को करते हुए सदैव ईश्वर का ध्यान करना लययोग है।
Hatha Yoga (हठ योग)
विभिन्न मुद्राओं, आसनों, प्राणायाम एवं बंधों के अभ्यास से शरीर को निर्मल एवं मन को एकाग्र करना हठयोग कहलाता है।
Raj Yoga (राज योग)
यम-नियमादि के अभ्यास से चित्त को निर्मल कर ज्योतिर्मय आत्मा का साक्षात्कार करना राजयोग कहलाता है। राज का अर्थ है दीप्तिमान, ज्योतिर्मय तथा योग का अर्थ समाधि अथवा अनुभूति है।
गीता में ध्यानयोग, सांख्ययोग, एवं कर्मयोग के बारे में विस्तृत विवेचन है। गीता के पंचम अध्याय में सन्यास योग एवं कर्मयोग में, कर्मयोग को श्रेष्ठ माना गया है।
Effects Of Yoga On Body (योग का शरीर पर प्रभाव )
Yoga – योग का अर्थ :
योग का अर्थ है अपनी चेतना (अस्तित्व ) का बोध। अपने अंदर निहित शक्तियों को विकसित करके परम चैतन्य आत्मा का साक्षात्कार एवं पूर्ण आनंद की प्राप्ति। इस यौगिक प्रक्रिया में विविध प्रकार की क्रियाओं का विधान हमारे ऋषि मुनियों ने किया है।
इन सभी क्रियाओं से हमारी सुप्त चेतना शक्ति का विकास होता है। सुप्त (डैड) तन्तुओं का पुनर्जागरण होता है एवं नए तन्तुओं कोशिकाओं का निर्माण होता है।
Yoga की सूक्ष्म क्रियाएं :
योग की सूक्ष्म क्रियाओं द्वारा हमारे सूक्ष्म स्नायुतंत्र को चुस्त किया जाता है, जिससे उनमें ठीक प्रकार से रक्त परिभ्रमण होता है और नयी शक्ति का विकास होने लगता है। योग से रक्त परिभ्रमण पूर्णरूपेण सम्यक रीति से होने लगता है। शरीर विज्ञान का यह सिद्धांत है कि शरीर के संकोचन व विमोचन होने से उनकी शक्ति का विकास होता है तथा रोगों का नाश होता है।
Yoga – Asanas & Pranayama (आसन व प्राणायाम)
आसन एवं प्राणायामों के द्वारा शरीर की ग्रंथियों व माँसपेशियों में विभिन्न योगिक क्रियाओं से उनका आरोग्य बढ़ता है। रक्त को वहन करने वाली धमनियाँ एवं शिराएँ भी स्वस्थ्य हो जाती हैं। पैंक्रियास एक्टिव होकर इन्सुलिन ठीक मात्रा में बनाने लगता है, जिससे डायबिटीज आदि रोग दूर होते हैं।
Yoga and Digestive System (योग और पाचन तंत्र)
पाचनतंत्र के स्वास्थ्य पर पूरे शरीर का स्वास्थ्य निर्भर करता है। सभी बीमारियों का मूल कारण पाचन तंत्र की अस्वस्थता है। यहाँ तक की ह्रदय रोग जैसी भयंकर बीमारी का कारण भी पाचन तंत्र का अस्वस्थ्य होना पाया गया है। योग से पाचनतंत्र पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाता है जिससे सम्पूर्ण शरीर स्वस्थ, हल्का व स्फूर्तिदायक बन जाता है।
योग से ह्रदय रोग जैसी भयंकर बीमारी से भी छुटकारा पाया जा सकता है।
फेफड़ो में पूर्ण स्वस्थ वायु का प्रवेश होता है जिससे फेफड़े स्वस्थ होते हैं तथा दमा, श्वास, एलर्जी आदि से छुटकारा मिलता है। जब फेफड़ों में स्वस्थ वायु जाती है तो उससे ह्रदय को भी बल मिलता है।
योग और मन :
योगिक क्रियाओं से मेद का पाचन होकर शरीर का भार कम होता है तथा शरीर स्वस्थ, सुडौल एवं सुन्दर बनता है। इतना ही नहीं, इस स्थूल शरीर के साथ-साथ योग सूक्ष्म शरीर एवं मन के लिए भी अनिवार्य है।
इस प्रकार हम योग का सहारा लेकर शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक एवं आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त कर सकते हैं।
स्वस्थ व्यक्ति की दिनचर्या —
सुस्वास्थ्य ही सम्पूर्ण सुखों का आधार है। स्वास्थ्य है तो जहान है, नहीं तो शमशान है। स्वस्थ कौन है ? आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रन्थ सुश्रुत में ऋषि लिखते हैं — जिसके तीनो दोष वात, पित्त और कफ सम हो, जठराग्नि सम हो (अर्थात न अति मंद न अति तीव्र), शरीर को धारण करने वाली सप्त धातुएँ रस, रक्त, माँस, मेद, अस्थि, मज्जा तथा वीर्य उचित अनुपात में हों, मल-मूत्र की क्रिया सम्यक प्रकार से होती हों और दस इन्द्रियाँ (कान, नाक, आँख, त्वचा, रसना, गुदा, उपस्थ, हाथ, पैर व जिव्हा), मन एवं इनका स्वामी आत्मा भी प्रसन्न हो तो ऐसे व्यक्ति को स्वस्थ कहा जाता है। ऋषियों ने स्वस्थ शब्द की बहुत ही व्यापक एवं वैज्ञानिक परिभाषा की है।
स्वस्थता की प्राप्ति हेतु आहार, निद्रा, एवं ब्रह्मचर्य तीन स्तम्भ हैं या आधार हैं जिनके ऊपर शरीर टिका हुआ है।
गीता में योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं, आहार, विहार, विचार एवं व्यवहार संतुलित व संयमित हैं, जिसके कार्यो में दिव्यता, मन में सदा पवित्रता व शुभ के प्रति अभीप्सा है, जिसका शयन एवं जागरण अर्थपूर्ण है, वही सच्चा योगी है।

संतुलित आहार
1. आहार :
आहार से व्यक्ति के शरीर का निर्माण होता है। आहार का शरीर पर ही नहीं मन पर भी पूरा प्रभाव पड़ता है। उचित मात्रा एवं ऋतु के अनुकूल भोजन करने वाला स्वस्थ रहता है।
प्रकृति अनुरूप भोजन :
अपनी प्रकृति(वात, पित्त, कफ) को जानकार उसके अनुसार भोजन लेना चाहिए। यदि वात प्रकृति है, शरीर में वायु विकार होते हैं तो चावल आदि वायुकारक एवं खट्टे भोजन का त्याग कर देना चाहिए। छोटी पिप्पली, सौंठ, अदरक आदि का प्रयोग करते रहना चाहिए।
पित्त प्रकृति वाले को गर्म, तले हुए पदार्थ नहीं लेने चाहिए। घीया, खीरा, ककड़ी आदि कच्चा भोजन लाभदायक होता है।
कफ प्रकृति वाले को ठंडी चीज़ें चावल, दही, छाछ आदि का सेवन अति मात्रा में नहीं करना चाहिए। दूध में छोटी पिप्पली, हल्दी आदि डालकर सेवन करना चाहिए।
भोजन की उचित मात्रा :
उचित मात्रा में भोजन करना चाहिए। आमाशय का आधा भाग अन्न के लिए, चतुर्थांश पेय पदार्थों के लिए रखते हुए शेष भाग वायु के लिए छोड़ना उचित है। ऋतु के अनुसार पदार्थों का मेल करके सेवन करने से रोग पास में नहीं आते हैं ।
भोजन का उचित समय :
भोजन का समय निश्चित होना चाहिए। असमय पर किया गया भोजन अपचन का कारण होता है।
प्रातः काल आठ से नौ के बीच हल्का पेय व फलादि लेना अच्छा है। प्रातः काल में अन्न का प्रयोग जितना कम हो शरीर के लिए उतना उत्तम है। पचास वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति प्रातराश न ले तो अच्छा है। मध्यान्ह में 11 से 12 बजे तक भोजन लेना उत्तम है। 12 से 1 बजे का समय मध्यम, उसके बाद उत्तरोत्तर निकृष्ट माना जाता है।
सांयकाल में भोजन सात से आठ का समय उत्तम, आठ से नौ का समय माध्यम और नौ बजे के बाद उत्तरोत्तर निकृष्ट समय होता है। भोजन करते समय वार्तालाप नहीं करना चाहिए। इसके साथ भोजन शांत भाव से चबाकर खाना चाहिए। एक ग्रास को बत्तीस बार या कम से कम बीस बार तो चबा कर खाना ही चाहिए।
भोजन करते समय पानी न पीना :
भोजन के बीच में पानी नहीं पीना चाहिए। यदि भोजन अटक रहा है तो 2-3 घूंट पी सकते हैं। भोजन के कम से कम 1 घंटा पश्चात पानी पीना श्रेष्ठ रहता है।यदि छाछ हो तो जरूर पीनी चाहिए।
ऐसा कहा जाता है कि जो प्रातः काल उठकर जलपान करता है, रात्रि के भोजनोपरांत दुग्धपान तथा मध्यान्ह के भोजन के बाद छाछ पीता है उसे वैद्य की आवश्यकता नहीं होती है। अर्थात वह व्यक्ति निरोगी रहता है।
इसके साथ साथ हमारा भोजन पूर्णरूप से हमारे लिए उपयुक्त होना चाहिए। भोजन में खनिज लवण व विटामिन भी भरपूर होना चाहिए।
2. निद्रा :
निद्रा अपने आप में एक पूर्ण सुखद अनुभूति है। यदि व्यक्ति को नींद न आये तो पागल भी हो सकता है। एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए 6 घंटे की नींद पर्याप्त होती है। बालक एवं वृद्ध के लिए 8 घंटे सोना उचित है। सांयकाल शीघ्र सोना व प्रातः काल शीघ्र उठना व्यक्ति के जीवन को उन्नत बनाता है।
3. ब्रह्मचर्य :
अपनी इन्द्रियों एवं मन को विषयों से हटाकर ईश्वर एवं परोपकार में लगाने का नाम ब्रह्मचर्य है। इन्द्रियों एवं मन की शक्तियों का रूपांतरण कर उनको आत्ममुखी कर ब्रह्म की प्राप्ति करना ब्रह्मचर्य है।

योग – व्यायाम
4. व्यायाम :
इस शरीर को चलाने के लिए जैसे आहार की आवश्यकता है वैसे ही आसन-प्राणायाम आदि व्यायाम की भी परम आवश्यकता है। बिना व्यायाम के शरीर अस्वस्थ तथा ओज एवं कांतिहीन हो जाता है। जबकि नियमित रूप से व्यायाम करने से दुर्बल, रोगी एवं कुरूप व्यक्ति भी बलवान, स्वस्थ एवं सुन्दर बन जाता है। ह्रदय रोग, मधुमेह, मोटापा, वात रोग, बवासीर, गैस, रक्तचाप, मानसिक तनाव आदि का भी मुख्य कारण शारीरिक श्रम का अभाव है। यदि नित्य प्रति योगाभ्यास किया जाए तो यह रोग कभी भी नहीं हो सकते।
व्यायाम के भी कई प्रकार हैं। इन सब में आसन प्राणायाम सर्वोत्तम है। दूसरे व्यायामों से शारीरिक परिश्रम तो होता है परन्तु मन में एकाग्रता एवं शांति नहीं आती। भारी व्यायाम करने से मांसपेशियों का ही व्यायाम होता है,स्नायु का व्यायाम नहीं होता। इसलिए भारी व्यायाम से मांसपेशियां इतनी सख्त हो जाती हैं कि उनमे धीरे-धीरे रक्त परिभ्रमण होना भी बंद हो जाता है तथा दर्द होना प्रांरभ हो जाता है। जबकि आसन-प्राणायाम से पूर्ण आरोग्य लाभ होता है तथा किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं होती तथा शरीर के साथ मन में एकाग्रता एवं शांति का विकास होता है।
5. स्नान :
आसन आदि के पश्चात शरीर का तापमान सामान्य होने पर स्नान करना चाहिए। स्नान से शरीर में ताज़गी आती है, अनावश्यक गर्मी शांत होकर शरीर शुद्ध एवं हल्का बन जाता है। जल से शरीर शुद्ध होता है। सत्य से मन की शुद्धि होती है। विद्या एवं तप के अनुष्ठान से आत्मा तथा ज्ञान से बुद्धि निर्मल बनती है। रोगी को छोड़कर सामान्य व्यक्ति को स्नान ठंडे पानी से करना चाहिए। गर्म पानी से स्नान करने पर मंदागिनी एवं दृष्टि दुर्बलता आदि रोग हो जाते हैं। असमय में ही बाल सफ़ेद होने व गिरने लगते हैं। शरीर में अनावश्यक गर्मी बढ़कर धातुक्षीणता होती है।

ध्यान
6. ध्यान :
शौच, स्नान, आसनादि नित्यकर्मों से निवृत होकर सुख, शांति एवं आनंद की कामना रखनेवाले व्यक्ति प्रतिदिन कम से कम 15 मिनट से लेकर 1 घंटे तक भगवान का ध्यान, उपासना अवश्य करें। गायत्री आदि मंत्रो का दीर्घकाल तक श्रद्धापूर्वक किया हुआ जप परमशक्ति, शांति व आनंददायक होता है।
इस प्रकार हम योग को अपनाकर जीवन में स्वस्थ्य रहने के साथ सम्पूर्ण ऊर्जा से भरकर अपने सभी कार्यो को और बेहतर ढंग से कर सकते हैं। क्योंकि मन एवं शरीर के स्वस्थ होने से हमारी प्रगति के रास्ते खुलते जाते हैं। आपको यह लेख कैसा लगा इसके बारे में अवश्य बताएं।